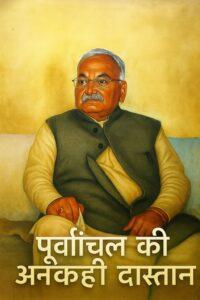यह लेख सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक आह्वान है। हिमालय की पुकार को सुनने का समय आ गया है, न केवल उन पर्वतों से आने वाली दिव्य ध्वनि को, बल्कि उनकी मूक चीत्कारों को भी जो हमारी उपेक्षा और लालच से मर रहे हैं। सच्ची भक्ति में साहस होता है,अपने प्रिय को बचाने का साहस, भले ही इसके लिए अपनी सुविधाओं का त्याग करना पड़े।


वित्र व्यापार की कड़वी सच्चाई
भारत एक गहरे विरोधाभास के चंगुल में फंसा है जो उसकी आध्यात्मिक पहचान की जड़ों को हिला रहा है। जिन हिमालयी शिखरों ने मानवता की सबसे गंभीर दार्शनिक परंपराओं को जन्म दिया, जिन पर्वतों ने ऋषियों के ध्यान और वेदों की रचना को साक्षी बनाया, वे आज उन्हीं लोगों के हाथों व्यवस्थित रूप से नष्ट हो रहे हैं जो यहां दैवी कृपा पाने का दावा करते हैं। हाल की घटनाएं इस संकट की गंभीरता को उजागर करती हैं: जुलाई 2025 में हिमाचल प्रदेश में 51 लोगों की मृत्यु और 30 से अधिक लापता, जबकि अगस्त 2025 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आकस्मिक बाढ़ में 5 लोगों की जान गई और 50 से अधिक लापता हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है; यह भूस्खलन की बढ़ती आवृत्ति, भूजल स्तर में गिरावट और पवित्र स्थलों के मनोरंजन पार्कों में बदलने के रूप में दिखने वाली मापी जा सकने वाली वास्तविकता है।
आंकड़े एक ऐसी कहानी कहते हैं जो तत्काल बौद्धिक चिंतन की मांग करती है। केदारनाथ, जो 2012 में 5 लाख तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रूप से आश्रय देता था, आज 25 लाख वार्षिक आगंतुकों के भार से कराह रहा है अपनी पारिस्थितिकी सहन क्षमता से तिगुना अधिक। वैष्णो देवी में तीर्थयात्रियों की संख्या 80 लाख से बढ़कर 1.2 करोड़ हो गई है, जो एक ऐसा पर्यावरणीय और ढांचागत संकट पैदा कर रहा है जिसका समाधान किसी भी मात्रा की भक्ति भावना केवल प्रार्थनाओं से नहीं कर सकती। जोशीमठ का धंसान संकट एक भयावह चेतावनी है ,2022-2024 के बीच यह शहर 30 सेमी तक धंस चुका है, जहां 868 से अधिक इमारतों में दरारें आई हैं और सैकड़ों परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं।
यह संकट केवल पर्यावरणीय क्षरण या पर्यटन के गलत प्रबंधन से कहीं अधिक गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में 2024 में 101 आपदाओं की घटनाएं हुईं जिनमें 37 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 2025 में केवल जुलाई-अगस्त में 170 से अधिक जानें गईं और ₹1,59,981 लाख का नुकसान हुआ। गंगोत्री मार्ग पर धराली गांव में आए अचानक बाढ़ ने दिखाया कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव गंभीरतम तीर्थ स्थलों तक पहुंच रहा है। यह एक मौलिक दार्शनिक असफलता का प्रतीक है: आध्यात्मिक अनुभव की मात्रा और गुणवत्ता के बीच, पहुंच और प्रामाणिकता के बीच, धार्मिक व्यापार और सच्ची तीर्थयात्रा के बीच अंतर न कर पाना।
पारिस्थितिकी पतन की शारीरिक संरचना
हिमालयी संकट कोई अमूर्त विषय नहीं है; यह विनाशकारी रूप से ठोस है। 2010 से 2020 के बीच, इस क्षेत्र में वनों की कटाई की दर 25% बढ़ी है, जो सीधे तौर पर पर्यटन ढांचे के विकास से जुड़ी है। यह कोई संयोगवश पर्यावरणीय परिवर्तन नहीं है , यह होटलों, पहुंच मार्गों और व्यावसायिक सुविधाओं के निर्माण से होने वाला व्यवस्थित आवास विनाश है जो सच्ची तीर्थयात्रा की आवश्यकताओं के बजाय बड़े पैमाने पर पर्यटन की सेवा करता है।
पानी के संकट पर विचार करें: मुख्य तीर्थ मार्गों पर प्राकृतिक जल स्रोतों में 60% की गिरावट सिर्फ सांख्यिकीय आंकड़ों से कहीं अधिक दर्शाती है। यह उन जल प्रणालियों के विघटन को दर्शाती है जिन्होंने हजारों वर्षों तक पर्वतीय समुदायों का पोषण किया है। जोशीमठ की धंसान का संकट कोयले की खान में कैनेरी पक्षी का काम करता है, यह दिखाता है कि अनियंत्रित निर्माण और अत्यधिक भूजल दोहन कैसे पवित्र भूगोल को उन लोगों के पैरों के नीचे से शाब्दिक रूप से गिरा सकता है जो आशीर्वाद की तलाश में आते हैं।
कचरा उत्पादन के आंकड़े:केवल बद्रीनाथ के पास सालाना 3,500 टन,यह दिखाते हैं कि कैसे उपभोक्ता संस्कृति ने उन स्थानों पर आक्रमण किया है जो परंपरागत रूप से त्याग और सादगी से परिभाषित होते थे। अलकनंदा नदी, जिसे लाखों लोग पवित्र मानते हैं, अब पैकेज्ड भोजन, प्लास्टिक की बोतलों और मानव अपशिष्ट का मलबा ढोती है जो उन तीर्थयात्रियों द्वारा पैदा किया जाता है जो आध्यात्मिक शुद्धीकरण की तलाश में आते हैं लेकिन भौतिक प्रदूषण में योगदान देते हैं।
ये धार्मिक भक्ति के अपरिहार्य परिणाम नहीं हैं। ये आध्यात्मिक उत्साह के रूप में छुपी नीतिगत असफलताएं हैं।
आध्यात्मिक शोषण की अर्थव्यवस्था
हिमालयी धार्मिक पर्यटन का वर्तमान मॉडल आर्थिक उपनिवेशवाद का एक रूप दर्शाता है जो संसाधन निष्कर्षण उद्योगों के पर्यवेक्षकों के लिए तुरंत पहचाना जा सकता है। लगभग 80% पर्यटन राजस्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं, कॉर्पोरेट टूर ऑपरेटरों और बाहरी सेवा प्रदाताओं के पास जाता है, जबकि स्थानीय समुदायों को केवल 20% हाउसकीपिंग और खाद्य सेवा में कम मजदूरी के रोजगार के माध्यम से मिलता है।
यह आर्थिक ढांचा एक विकृत प्रोत्साहन प्रणाली बनाता है। जितने अधिक तीर्थयात्री आते हैं, उतना ही अधिक पर्यावरणीय नुकसान होता है, लेकिन लाभ उन संस्थाओं को मिलता है जिनकी क्षेत्र के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य में कोई दीर्घकालिक हिस्सेदारी नहीं है। स्थानीय समुदाय लागत उठाते हैं,पानी की कमी, ढांचागत दबाव, सांस्कृतिक विघटन,जबकि बाहरी अभिकर्ता मुनाफा कमाते हैं।
टिकाऊ विकल्पों के साथ तुलना एकदम स्पष्ट है। होमस्टे-आधारित पर्यटन मॉडल का विश्लेषण दिखाता है कि जब पर्यटन बुनियादी ढांचा समुदाय के स्वामित्व और संचालन में होता है तो 90% राजस्व स्थानीय समुदायों के भीतर ही रह सकता है। एक पारंपरिक पहाड़ी होमस्टे दैनिक लगभग 10,000 लीटर पानी का उपयोग करता है जबकि एक बड़े होटल की तुलना में 200,000 लीटर, अधिक प्रामाणिक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हुए और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन पैदा करता है।
रूपांतरण के लिए आर्थिक तर्क सम्मोहक है: वर्तमान पर्यटन अर्थव्यवस्था के केवल एक हिस्से को समुदाय-आधारित होमस्टे की ओर मोड़ना पर्यावरणीय प्रभाव को नाटकीय रूप से कम करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए सालाना ₹10,000 करोड़ पैदा कर सकता है।
सांस्कृतिक हानि का आकलन
शायद बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन का सबसे कपटी पहलू उन सांस्कृतिक परंपराओं का व्यवस्थित क्षरण है जिनका वह जश्न मनाने का दावा करता है। तीर्थयात्रा का वस्तुकरण गहरे आध्यात्मिक अभ्यासों को सतही उपभोक्ता अनुभवों में बदल देता है, जटिल धर्मशास्त्रीय परंपराओं को फोटो के अवसरों और सोशल मीडिया सामग्री में कम कर देता है।
ऐपन कला और ऊनी शॉल बुनाई जैसे पारंपरिक शिल्प—स्वदेशी पर्वतीय संस्कृति की अभिव्यक्तियां जो कभी स्थानीय समुदायों को आर्थिक जीविका प्रदान करती थीं,गायब हो रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर पर्यटन प्रामाणिक सांस्कृतिक उत्पादों के बजाय सस्ती, बड़े पैमाने पर उत्पादित स्मृति चिह्नों की मांग पैदा करता है। मौखिक कहानी सुनाने की परंपराएं, अनुष्ठानिक प्रथाएं, और मौसमी पालन जो कभी तीर्थयात्रा को गहरी पारिस्थितिकी और आध्यात्मिक लयों से जोड़ते थे, साल भर की व्यावसायिक पहुंच के पक्ष में छोड़ दिए जा रहे हैं।
यह सांस्कृतिक खनन का एक रूप दर्शाता है: परंपरा के सतही प्रतीकों को निकालना जबकि उन अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों को नष्ट करना जिन्होंने सदियों तक उन परंपराओं को बनाए रखा।
तीर्थयात्रा वर्गीकरण की अनिवार्यता
इस संकट को संबोधित करने के लिए बौद्धिक साहस की आवश्यकता है यह स्वीकार करने के लिए कि सभी धार्मिक पर्यटन समान आध्यात्मिक या सामाजिक उद्देश्यों की सेवा नहीं करते। एक विचारशील वर्गीकरण प्रणाली सच्चे आध्यात्मिक साधकों और आकस्मिक धार्मिक पर्यटकों के बीच अंतर कर सकती है, अलग-अलग पहुंच नीतियां बनाकर जो प्रामाणिक तीर्थयात्रा को प्राथमिकता देती हैं जबकि मनोरंजक दर्शन का प्रबंधन करती हैं।
ऐसी प्रणाली आगंतुकों को आध्यात्मिक तीर्थयात्रियों (मुख्यतः वृद्ध व्यक्ति जो मोक्ष की तलाश में हैं, प्राथमिकता पहुंच और अनुदानित दरों के हकदार), धार्मिक पर्यटकों (सामान्य आगंतुक कोटा प्रणालियों और बाजार दर मूल्य निर्धारण के अधीन), और सांस्कृतिक पर्यटकों (अवकाश-केंद्रित आगंतुक प्रतिबंधित मंदिर पहुंच के साथ लेकिन बेहतर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ) के रूप में वर्गीकृत कर सकती है।
यह दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण नहीं है; यह इस बात की व्यावहारिक पहचान है कि अलग-अलग प्रेरणाओं के लिए अलग-अलग प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। जिस तरह चिकित्सा प्रणालियां आवश्यकता की गंभीरता के आधार पर रोगियों का वर्गीकरण करती हैं, तीर्थयात्रा प्रबंधन को आध्यात्मिक इरादे और पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर पहुंच को प्राथमिकता देनी चाहिए।
आर्थिक न्याय के रूप में होमस्टे क्रांति
कॉर्पोरेट होटल प्रभुत्व से समुदाय-आधारित होमस्टे की ओर संक्रमण केवल पर्यटन नीति सुधार से अधिक दर्शाता है—यह आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को स्थानीय सशक्तिकरण के साथ जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण इस दृष्टिकोण की व्यवहार्यता दिखाते हैं: भूटान की उच्च-मूल्य, कम-मात्रा पर्यटन रणनीति ने कार्बन-नकारात्मक स्थिति बनाए रखते हुए टिकाऊ राजस्व उत्पन्न किया है, और जापान के कुमानो कोडो तीर्थ मार्ग होमस्टे नेटवर्क का उपयोग करते हैं जिन्हें यूनेस्को मान्यता मिली है।
कार्यान्वयन के लिए व्यवस्थित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। चरण एक (2024-2026) यमुनोत्री और गंगोत्री जैसी कम-दर्शित साइटों में पायलट कार्यक्रम स्थापित कर सकता है, प्रमाणित इको-होमस्टे के लिए 50% कर छूट प्रदान करता है। चरण दो (2027-2030) प्रमुख मंदिरों के 10 किलोमीटर के भीतर पूर्ण होटल निर्माण प्रतिबंध लागू करेगा जबकि राज्य-संचालित होमस्टे प्रमाणन कार्यक्रम विकसित करेगा। चरण तीन (2031+) सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत एक राष्ट्रीय हिमालयी होमस्टे नेटवर्क बनाएगा।
आर्थिक अनुमान सुझाते हैं कि यह दृष्टिकोण 2030 तक 200,000 होमस्टे इकाइयों का समर्थन कर सकता है, पारंपरिक शिल्प और सांस्कृतिक सेवाओं में 5 लाख नौकरियां पैदा करते हुए वार्षिक ₹10,000 करोड़ का प्रत्यक्ष स्थानीय आय उत्पन्न कर सकता है।
आध्यात्मिक लोकतंत्रीकरण के रूप में प्रौद्योगिकी
भौतिक पहुंच को सीमित करने और धार्मिक समावेशिता बनाए रखने के बीच स्पष्ट विरोधाभास को बुद्धिमान प्रौद्योगिकी तैनाती के माध्यम से हल किया जा सकता है। वर्चुअल दर्शन प्लेटफॉर्म और मैदानी क्षेत्रों में “मिनी धाम” प्रतिकृति साइटें नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव कम करते हुए आकस्मिक भक्तों की आध्यात्मिक जरूरतों की सेवा कर सकती हैं।
यह आध्यात्मिक समझौता नहीं है—यह इस पहचान है कि कई लोग जो दिव्य उपस्थिति पर्वतीय मंदिरों में खोजते हैं, वह उन लोगों के लिए तकनीकी मध्यस्थता से कम नहीं होती जिनकी प्राथमिक प्रेरणा तीर्थ यात्रा के बजाय दर्शन है। जिस तरह धार्मिक समारोहों का लाइव टेलीविजन प्रसारण लाखों भक्तों की सेवा करता है जो भौतिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, वर्चुअल और प्रतिकृति अनुभव भक्तिपूर्ण जरूरतों को संतुष्ट कर सकते हैं जबकि गंभीर आध्यात्मिक अभ्यास करने वालों के लिए पवित्र स्थलों को संरक्षित कर सकते हैं।
इको-धर्मशास्त्र एकीकरण चुनौती
टिकाऊ तीर्थयात्रा नीति के सबसे बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण पहलू में पर्यावरणीय चेतना को धार्मिक परंपरा के साथ एकीकृत करना शामिल है। इसके लिए परिष्कृत धर्मशास्त्रीय सहभागिता की आवश्यकता है जो प्रदर्शित करे कि पारिस्थितिकी विनाश आध्यात्मिक उद्देश्यों का विरोध करता है न कि सेवा।
वैदिक साहित्य में व्यापक पर्यावरण संरक्षण सिद्धांत हैं जो टिकाऊ तीर्थयात्रा प्रथाओं के लिए शास्त्रीय आधार प्रदान कर सकते हैं। स्थापित धार्मिक प्राधिकरणों के साथ साझेदारी “ग्रीन यात्रा” को धार्मिक अभ्यास पर लगाई गई धर्मनिरपेक्ष पर्यावरणीय नीति के रूप में नहीं, बल्कि प्रामाणिक आध्यात्मिक सिद्धांतों की वापसी के रूप में प्रस्तुत कर सकती है जो प्राकृतिक प्रणालियों में दिव्य उपस्थिति को पहचानते हैं।
यह दृष्टिकोण पर्यावरणीय नियमन को बाहरी बाधा से आंतरिक आध्यात्मिक अनुशासन में बदलता है, केवल सरकारी प्रवर्तन पर निर्भर रहने के बजाय टिकाऊ व्यवहार के लिए धार्मिक प्रेरणा पैदा करता है।
जोखिम आकलन और शमन रणनीतियां
रूपांतरकारी तीर्थयात्रा नीति के कार्यान्वयन को स्थापित वाणिज्यिक हितों, पर्यटन राजस्व पर निर्भर राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों, और असीमित पहुंच के आदी तीर्थयात्रियों से अनुमानित प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। सफल संक्रमण के लिए दीर्घकालिक स्थिरता उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए इन वैध चिंताओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।
राजनीतिक प्रतिरोध को होमस्टे और कारीगर सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय रोजगार सृजन पर जोर देकर कम किया जा सकता है, यह दिखाते हुए कि टिकाऊ पर्यटन कॉर्पोरेट होटल मॉडल की तुलना में अधिक वितरित आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है। तीर्थयात्रियों के विरोध को स्तरीकृत पहुंच प्रणालियों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है जो क्षमता प्रबंधन के कार्यान्वयन करते हुए उपलब्धता बनाए रखती हैं, अमरनाथ में सफल मॉडल के समान जहां दैनिक सीमा स्वीकृत प्रथा बन गई है।
होमस्टे मानकों के बारे में गुणवत्ता नियंत्रण की चिंताओं को केरल के जिम्मेदार पर्यटन मिशन पर आधारित व्यापक प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, “रुद्राक्ष रेटिंग” प्रणाली बनाकर जो सांस्कृतिक प्रामाणिकता बनाए रखते हुए सुसंगत सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।
कार्य के लिए नैतिक आवश्यकता
हिमालयी धार्मिक पर्यटन संकट अंततः एक नैतिक प्रश्न उठाता है जो नीतिगत प्राथमिकताओं या आर्थिक गणनाओं से कहीं आगे तक फैलता है: क्या हमारा नैतिक दायित्व है कि हम पवित्र परिदृश्यों और प्रामाणिक आध्यात्मिक परंपराओं को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें, भले ही ऐसा करने के लिए वर्तमान उपभोग पैटर्न को सीमित करना पड़े?
यह उत्तर तीर्थयात्रा के गहरे उद्देश्यों पर विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्पष्ट होना चाहिए। पवित्र स्थलों की भौतिक यात्रा आध्यात्मिक विकास की सेवा इसलिए करती है क्योंकि इसमें अनुशासन, त्याग और प्राकृतिक सीमाओं के प्रति सम्मान शामिल होता है। बड़े पैमाने पर पर्यटन जो इन चुनौतियों को समाप्त करता है, उन आध्यात्मिक लाभों को भी समाप्त करता है जिन्होंने यात्रा को उचित ठहराया था।
अधिक मौलिक रूप से, भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को प्रेरणा देने वाले परिदृश्यों का विनाश सांस्कृतिक आत्महत्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये पर्वत केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए सुंदर पृष्ठभूमि नहीं हैं,ये उन धर्मशास्त्रीय और दार्शनिक प्रणालियों के अभिन्न अंग हैं जिनका अनुभव तीर्थयात्री करना चाहते हैं। पर्यावरणीय क्षरण आध्यात्मिक उद्देश्यों को सीधे तौर पर कमजोर करता है।
कार्यान्वयन पथ और तात्कालिकता आकलन
हिमालयी धार्मिक पर्यटन के रूपांतरण के लिए पायलट कार्यक्रमों के तत्काल कार्यान्वयन की आवश्यकता है जबकि दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन विकसित होते हैं। यमुनोत्री होमस्टे जोन पायलट बारह महीने के भीतर शुरू हो सकता है, व्यापक विस्तार के लिए प्रदर्शन मॉडल प्रदान करता है। वर्चुअल दर्शन प्लेटफॉर्म और मिनी धाम प्रतिकृति साइटों का समवर्ती विकास भौतिक साइट बहाली आगे बढ़ने के दौरान आकस्मिक पर्यटन मांग को अवशोषित करना शुरू कर सकता है।
तात्कालिकता को कम करके नहीं आंका जा सकता। व्यवस्थित हस्तक्षेप के बिना प्रत्येक गुजरता पर्यटन सीजन पर्यावरणीय क्षति, सांस्कृतिक क्षरण और आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन अधिक अप्रत्याशित मौसम पैटर्न बनाकर इन दबावों को बढ़ाता है जो पर्यटन और स्थानीय आजीविका दोनों को अधिक अनिश्चित बनाते हैं।
फिर भी अवसर उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत टिकाऊ धार्मिक पर्यटन में वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर सकता है, दुनिया भर के पवित्र स्थलों पर लागू मॉडल बनाते हुए यह प्रदर्शित कर सकता है कि पारंपरिक ज्ञान समकालीन नीतिगत चुनौतियों को कैसे सूचित कर सकता है।
विरासत और वाणिज्य के बीच चुनाव
हिमालयी तीर्थयात्रा संकट अल्पकालिक व्यावसायिक शोषण और दीर्घकालिक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच एक मौलिक चुनाव के लिए मजबूर करता है। इस चुनाव को अनिश्चित काल तक विलंबित नहीं किया जा सकता जबकि नीति समितियां अतिरिक्त अध्ययन करती हैं या हितधारक समूह वृद्धिशील समझौतों पर बातचीत करते हैं।
आगे का रास्ता वर्तमान प्रथाओं के विनाशकारी परिणामों के बारे में बौद्धिक ईमानदारी, वाणिज्यिक विरोध के बावजूद आवश्यक प्रतिबंध लागू करने का नैतिक साहस, और स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हुए प्रामाणिक आध्यात्मिक जरूरतों की सेवा करने वाले टिकाऊ विकल्प डिजाइन करने की रचनात्मक दृष्टि की आवश्यकता है।
लक्ष्य धार्मिक पर्यटन को समाप्त करना नहीं है बल्कि इसे सच्ची तीर्थयात्रा में बदलना है जो उस पवित्र भूगोल और उन समुदायों दोनों का सम्मान करे जो इसकी यात्रा करती है और जो इसकी पहुंच बनाए रखते हैं। यह रूपांतरण केवल पर्यटन नीति सुधार से कहीं अधिक दर्शाता है,यह समकालीन चुनौतियों के लिए पारंपरिक ज्ञान को लागू करने की संभावना को मूर्त रूप देता है, यह दिखाता है कि आध्यात्मिक सिद्धांत जटिल समस्याओं के व्यावहारिक समाधान को सूचित कर सकते हैं।
हिमालय जिन्होंने सभी अस्तित्व की मौलिक परस्पर संबद्धता की घोषणा करने वाले ग्रंथों की रचना को देखा है, वे ऐसे नीतिगत निर्णयों की प्रतीक्षा में हैं जो इन गहरी अंतर्दृष्टियों का विरोध करने के बजाय प्रतिबिंबित करते हैं। टिकाऊ कार्य करने का चुनाव स्वयं में तीर्थयात्रा का एक रूप है,तत्काल संतुष्टि से कहीं महान उद्देश्यों की सेवा करने वाले ज्ञान की ओर एक कठिन यात्रा। ऐसी तीर्थयात्रा का समय अब है।